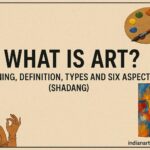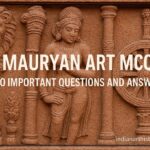लगभग 1905 से 1920 तक बंगाल शैली बड़े जोरों से पनपी देश भर में इसका प्रचार हुआ और इस कला-आन्दोलन को राष्ट्रीय कहा गया।
1920 के लगभग इस क्षेत्र में एक नया मोड़ आया एक कारण तो यह था कि अवनीन्द्रनाथ के सामने केवल मुगल तथा अजन्ता शैली का ही आदर्श था।
उस समय तक अन्य शैलियों की चित्रकला की खोज पूर्ण नहीं हुई थी। पीछे से जब राजस्थानी, पहाड़ी तथा अपभ्रंश शैलियों की विस्तृत खोज हुई तो अवनीन्द्रनाथ की एकांगिता समझ में आने लगी।
भारतीय कला के इन विभिन्न प्राचीन रूपों का अध्ययन करके समयानुकूल शैली का निर्माण करना बड़ा कठिन था।
दूसरा कारण यह था कि विदेशों से भारत का सम्पर्क होने के कारण तथा भारतीय कलाकारों के विदेश भ्रमण के कारण यूरोप की नई-नई शैलियों का भारत में आगमन हुआ।
कलाकारों के सामने दो ही विकल्प रह गये : या तो वे आधुनिक कला को अपनायें या प्राचीन शैलियों का अनुकरण करें।
सन् 1930 में रवीन्द्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी हुई। गगनेन्द्रनाथ ने लगभग इसी समय घनवादी शैली में अनेक चित्र बनाये। 1925 के लगभग यामिनीराय ने बंगाल की लोक-कला के आधार पर नये प्रयोग किये।
सन् 1933 में लंका में जार्ज कीट ने भी एक नई शैलो का आरम्भ किया। इन सबने ठाकुर शैली को असामयिक कर दिया; किन्तु ठाकुर शैली को सबसे बड़ा आघात पहुँचा अमृता शेरगिल की कला से, जिन्होंने भारत आकर 1935 में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की।
आरम्भ में उनका बड़ा विरोध हुआ और उनकी कला को अभारतीय कहा गया, किन्तु धीरे-धीरे उनकी आधुनिकता और भारतीयता समझ में आने लगी।
इन सब प्रयोगों से भारतीय कला अनेक नये-नये मार्गों पर चलने लगी। आरम्भ में यद्यपि कुछ विदेशी शैलियों की नकल भी हुई किन्तु अवनीन्द्रनाथ की कला द्वारा उत्पन्न की हुई राष्ट्रीय भावना ने विदेशी शैलियों के तूफान को भारत में चलने से रोक दिया।
कलाकार अपनी कला में मौलिकता और भारतीयता की आवश्यकता अनुभव करने लगे। फलस्वरूप आज भारत की चित्रकला जहाँ आधुनिकता में किसी भी देश से पीछे नहीं है वहाँ वह मौलिकता और भारतीयता में भी किसी से घटकर नहीं है।
Table of Contents
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (1861-41 ई०)
विश्व मंच पर कवि के रूप में विख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता के एक सम्भ्रान्त परिवार में 7 मार्च 1861 ई० को हुआ था यह परिवार पश्चिमी सभ्यता एवं विचारों, ईस्ट इण्डिया कम्पनीके ब्रिटिश उच्च अधिकारियों आदि के निरन्तर सम्पर्क में रहा था।
कम्पनी के साथ-साथ इस परिवार की समृद्धि भी बढ़ती गयी तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पितामह प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के समय वह उन्नति के चरम शिखर पर थी।
द्वारकानाथ ठाकुर प्रगतिशील विचारों के थे 1784 ई० में सर विलियम जोन्स के साथ उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना की जिसके द्वारा आर्कियोलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया तथा इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता का आरम्भ किया गया ।
वे समाज-सुधार के क्षेत्र में राजा राममोहनराय के समर्थक थे और कलाओं में रूचि लेते थे। रवीन्द्रनाथ के पिता देवेन्द्रनाथ आध्यात्मिक तत्ववादी थे। उनकी माता का देहान्त उनके शैशव में ही हो गया था।
रवीन्द्रनाथ के परिवार में दार्शनिक, विद्वान, कलाकार, समाज सुधारक तथा प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति थे। विदेशी साहित्य से भी उनका घर भरा रहता था।
रवीन्द्रनाथ पर इन सबका प्रभाव पड़ा और वे कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक तथा चित्रकार आदि अनेक प्रकार का व्यक्तित्व स्वयं में विकसित कर सके।
उन्होंने कलकत्ता की बंगाल अकादमी तथा लन्दन के यूनीवर्सिटी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। उनका शेष समस्त जीवन परिवार तथा मित्रों के प्रभाव से ही उनके बहुमुखी विकास का द्योतक है।
सन् 1901 में उन्होंने शान्ति निकेतन की स्थापना की। 1905 ई० में स्वदेशी आन्दोलन में व्यस्त रहे यद्यपि वे विदेशी वस्तुओं तथा विचारों के बहिष्कार के पक्षपाती नहीं थे। 1907 में इण्डियन सोसाइटी आफ ओरिएण्टल आर्ट की स्थापना में सहयोग दिया ।
1912-13 में वे इंग्लैंड गये और 1913 में उन्हें “गीतांजलि” पर नोबेल पुरस्कार मिला। इससे उनकी ख्याति विश्वभर में फैल गयी। 1915 से 1919 तक विचित्रा क्लब का संचालन किया।
उन्होंने बंगाल शैली की आलोचना की और उसमें अनेक कमियाँ बतायीं। 1915 में ही वे जापान गये। 1919 में शान्ति निकेतन में कला भवन की स्थापना की।
1920 में वहाँ उन्होंने एक कला प्रतियोगिता आयोजित की, उसमें भाग भी लिया और निर्णायक भी बने । इसी वर्ष उन्होंने यूरोप का विस्तृत भ्रमण किया तथा निकोलस रोरिक से भी मिले। यूरोप में आधुनिक कला के नवीन आन्दोलनों से परिचित हुए।
1924 में जापान और चीन होते हुए अर्जेण्टाइना गये । 1926 में वे पुनः यूरोप यात्रा पर गये और प्रथम विश्व युद्ध के विरूद्ध लेख लिखे ।
यहीं मे ये चित्रकला के प्रति विशेष आकर्षित हुए। वे दिन-रात चित्र बनाने लगे और कविता आदि लिखना छोड़ दिया। 1930 ई० में उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई ।
इसी वर्ष उनकी अन्य प्रदर्शनियाँ बिरमिंघम सिटी, लन्दन, बर्लिन, ड्रेसडेन, म्यूनिख डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड, मास्को तथा न्यूयार्क में हुई। सभी जगह उनकी कला की प्रशंसा की गयी और आधुनिक भारत के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध हो गये। |
भारत में उनके चित्रों की प्रदर्शनी 1931 में बम्बई में तथा 1932 में कलकत्ता में हुई ।
भारत तथा विदेशों में उनकी अनेक प्रदर्शनियों 1931 से 34 तक और 1938 से 39 तक की अवधि में लगी। 7 अगस्त सन् 1941 को उन्होंने पार्थिव देह को त्याग दिया ।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कला-रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने वृद्धावस्था में लगभग 1920 से ही चित्रांकन आरम्भ किया था । इसका आरम्भ भी कविताओं की काट-छाँट तथा खरोंच की आकृतियों में विचित्र काल्पनिक रूप देखने से आरम्भ हुआ ।
इन्हीं के आधार पर उनके प्रयोग आरम्भ हुए । उनके माध्यम भी विचित्र थे। कागज पर फूल घिसकर फूल का रंग भरते, हल्दी से स्वर्ण की आभा दिखाने का प्रयत्न करते आर प्रखर सूर्य की किरणें दिखाने के अभिप्राय से कागज का वह स्थान रिक्त छोड़ देते।
उन्होंने कला के स्थापित नियमों का अनुपालन नहीं किया। उनके चित्रांकन के तन्त्र और शैली पूर्णतः व्यक्तिगत थे। लय की अनुभूति को ही वे कला का सबसे अधिक आवश्यक गुण मानते थे।
प्रकृति तथा पशुओं के प्रति उनके संवेदन बड़े गहरे थे, उससे उनकी कुछ आकृतियों में डरावनापन आ गया है। उन्होंने जीवन के रूखे और भयानक पक्षों को भी चित्रित किया है।
उनके समस्त चित्रों में कोणीयता अधिक है। सारे संसार में उनके चित्रों की प्रशंसा हुई पर स्वयं रवीन्द्रनाथ ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे चित्रों में क्या है।
आर्चर ने रवीन्द्रनाथ की कला की तीन विशेषताएँ मानी हैं:
1. उनकी कला पूर्ण रूप से आधुनिक है किन्तु आधुनिकता की दृष्टि से उसमें विश्व के किसी भी देश अथवा कलाकार की अनुकृति नहीं है।
2. भारतीय रेखाओं तथा आकृतियों का आधार लिया गया है। अतः पूर्ण रूप से भारतीय है।
3. वह पूर्णतः मौलिक है उसमें ताजगी और शक्ति है।
जया अप्पासामी ने रवीन्द्रनाथ की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया
(1) सहजता उनकी कोई भी आकृति पूर्व-निश्चित नहीं है। –
(2) चित्रण की अपूर्णता फिनिश तथा तकनीकी परिष्कार का अभाव कहीं-कही रिक्त स्थान भी छोड़ दिया गया है।
(3) सजीवता चित्रों की आकृतियाँ ही नहीं वरन् सम्पूर्ण धरातल ही सजीव प्रतीत होता है।
(4) गम्भीर तथा चमकविहीन रंग इनमें रहस्यात्मकता भी प्रतीत होती है।
(5) सभी आकृतियों में लयात्मकता है।
(6) धरातलों तथा आकृतियों में टेक्सचर की विविधता है जिसे आधुनिक कला से पहले कभी भी प्रशंसित नहीं किया गया था।
(7) कुछ चित्रों में अंधेरे के विपरीत तेज चमक अथवा प्रकाश का प्रभाव चमकीली पृष्ठभूमियों में अंधेरी आकृतियाँ ।
(8) विषयों की अपेक्षा रचना-विधि की प्रमुखता रेखांत्मक चित्रों में पेन, पेंसिल या फ्रेयन के प्रभाव। रंगीन चित्रों में धब्बों का प्रयोग चित्रों में अन्धकार की अधिकता ।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कला का विकास कई चरणों में हुआ है। इस विकास को बालक की कलासे लेकर मानव की कला तक का विकास कहा गया है।
स्वयं रवीन्द्रनाथ ने तो केवल यही कहा कि लोग अक्सर मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं किन्तु अपने चित्रों की भाँति में भी चुप रहता हूँ।
इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि वृद्धावस्था में उन्होंने चित्रकार के रूप में जो जीवन व्यतीत किया वह दूसरे बचपन के समान था ।
उनकी कला का विकास इस दूसरे बचपन के बालक की कला से मनुष्य की कला तक हुआ है उनकी सम्पूर्ण कला का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मानवता स्वयं को कलाभिव्यक्ति के द्वारा मुक्त अनुभव कर सकती है और अन्तःकरण में हजारों वर्ष से छिपे मनोभावों को रूप दे सकती है।
यदि मनुष्य बुद्धि के अहंकार को हावी न होने दे। हम दूसरे रूपों की अनुकृति न करें बल्कि आन्तरिक लय के अनुसार ही सृजन करें।
बुद्धि के चक्कर से मुक्त रहकर बालक विचित्र रूपों और दिवा स्वप्नों का अधिक काल्पनिक आनन्द ले सकते हैं यदि कोई वयस्क भी तर्क बुद्धि की कठोरता को छोड़ दे तो इसका आनन्द ले सकता है।
68 वर्ष की आयु में चित्रांकन करने के कारण रवीन्द्रनाथ ठाकुर में भी यह क्षमता आ गयी थी कि वे पुनः बालक के समान सहज हो जायें।
चित्रांकन आरम्भ करने वाला बालक पहले चील-विलार करता है और अलग-अलग ढंग से वक्र रेखाएँ खींचने का प्रयत्न करता है।
टैगोर ने अपनी कविताओं के कटे हुए अंशों में स्थान-स्थान पर अपने अचेतन मन के प्रभाव में रेखाओं की खींचतान से चील विलार आकृतियाँ बनायी हैं।
मन में कहीं तनिक-सा भी विकार होने पर उसे तुरन्त किसी रेखा में व्यक्त कर दिया, अत्यन्त संवेदनशील व्यक्ति की भाँति और प्रत्येक संवेदन को अपना सहज स्वाभाविक रूप ग्रहण करने दिया।
इस विधि से बनायी गयी रेखाओं में ऐन्द्रिक कल्पना भी है और भावात्मक प्रभाव भी ।
बाद में बनाये गये कुछ रूपों में तो मूर्तियों जैसा गुण भी झलकने लगा है लगता है मानों वे अपनी कल्पनाओं को छू लेना चाहते थे।
अपनी इन सभी आकृतियों में उन्होंने अंगुलियों, पेंसिल के टुकड़ों, रंगों तथा वस्तुओं को चिपकाने का माध्यम अपनाया है।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की यह आकृतियों बालकों की अपेक्षा कुछ अधिक शुद्धता तथा सफाई से बनायी गयी हैं। इसे परिष्कृत बाल कला कहा जा सकता है।”
1. If the comparison with the impulses of a child painter be significant, to any extent, the paintings of Rabindranath Tagore may be called sophistcated child art, much more accurately than similar work of the many advanced artists who have surrendered themselves to the methods of child art.
-Mulkraj Anand
बालक द्वारा खींची जाने वाली प्रथम आड़ी-तिरछी रेखाओं का कोई अर्थ नहीं होता, केवल तनाव से मुक्ति का लक्ष्य रहता है।
उसमें केवल एक प्रवाह रहता है, मानों अचेतन की ऊबड़-खाबड़ भूमि पर कोई धारा इधर-उधर भटकती सी बह रही हो किन्तु बालक रवीन्द्रनाथ के मन में असंख्य स्मृतियाँ संचित थीं उनका अहं इनसे पूर्णतः मुक्त होकर अरूप रेखाओं के आनन्द में उलझ कर नहीं रह सका।
उनकी कला में उनके चेतन मन का दबाव प्रकट होने लगा। वे एक बिन्दु से दूसरे बिन्दुको जोड़कर, आवर्तित या प्रत्यावर्तित रेखाओं, वर्गों, त्रिभुजों आदि को रूप देने लगे।
वे रूपों के अंकन की अकुशलता से छटपटा कर लयात्मक संयोजनों की ओर मुड़ गये। यहाँ तक उनकी कला में सादृश्य रूप प्रकट नहीं हुए। अरूप अरूप ही रहा।
पर वे स्याही से कुछ न कुछ रचना करते गये, कुछ ऐसी रचना जो उनकी आत्मा की आकुलता को प्रतीकात्मकता दे सके।
लम्बी बड़ी चाँच, वर्गाकार आँख, सीधी रेखा में बना समतल शिर, जिसमें समकोणीय व्यवस्था है, नीचे बनाये गये एक बराबर के खाने आदि आकृतियों अपने लघु या वृहद् आकार, सजीवता, ओज, परिप्रेक्ष्य रहित दृष्टि-बिन्दु और अपने अंकन की युक्ति (स्कीमा) आदि के द्वारा अचेतन की गहरी परतों को उखाड़ते गये बड़ी-बड़ी आँखों और बड़े मुँह वाले बड़े-बड़े साँप, मन के अँधेरे में से कागज पर प्रकट हो गये हैं ।
उनकी स्याही कुछ ऐसे रूप अंकित करने लगी जिसमें उनके मन की चीत्कार संगति देखना चाहती थी किन्तु इच्छाएँ ऊर्ध्वमुखी लय चाहती थीं।
रवीन्द्रनाथ की आकृतियों में परिप्रेक्ष्य नहीं आया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने पार्श्व …मुख अंकित किये।
आकृतियाँ श्रृंखलाबद्ध या वर्तुल संयोजनों में बनायी गयीं और महत्वपूर्ण रूप को बड़ा आकार दिया गया। रेखाओं आदि से बनाये गये रूपों के ऊपरी भाग में मुखाकृति जोड़कर मानवीय रूपों का आभास दिया गया है।
कुछ समय पश्चात् रवीन्द्र की आकृतियाँ स्पष्ट मानवीय रूप लेने लगीं । इन रूपों में उनकी दमित वासनाओं की पूर्ति वाले रूप भी हैं। मानों रात में भूत-प्रेत दिखाई दे रहे हों ।
ये आकृतियाँ प्रायः लम्बी या अण्डाकृति में हैं। कुछ साड़ी पहने जैसी लगती है। चारों ओर अँधेरी गहरी नीली पृष्ठभूमि में फीके चाँद जैसी पीली आकृतियाँ – उन अतृप्तियों के अवशेष, जो उनके मन में छिपे रहे।
इनके रंग उनकी इच्छाओं के प्रतीक हैं, रूप अतीत से जुड़े हुए हैं अतः प्रेतों के समान डरावने भी हो गये हैं।
इसके अन्तर के रूपों में व्यंजना बढ़ती गयी है। स्पष्ट रेखाओं, पुनरावृत्तियों तथा कोणों के द्वारा वे अपने आवेशों को व्यंजित करने लगे हैं।
मूल रंगों के द्वारा उदासी, क्रोध, भय आदि की भी व्यंजना हुई है। मनमें छिपे चेहरे उभर आये हैं जो कभी उनके प्रेम जगत की कल्पना में रहे थे, या जिनके प्रति आकर्षण तो था पर जिन्हें कभी स्पर्श नहीं किया जा सका था। इनमें उनके युवा काल की स्मृतियाँ हैं।
पर ये रूप सुन्दर नहीं बने, बल्कि टेढ़े-मेढ़े और कठोर हैं। समान्तर रेखाओं के बीच कोमल आँख, काठ जैसे होंठ, शायद किसी निर्दयता के संकेत है।
रंगों में कुछ गम्भीरता आयी है जिसने चित्रों की भयंकरता को और भी बढ़ा दिया है। फिर आयी है नाटकीयता ।
वेदना के कारण क्रन्दन करती ऊँट की आकृति, नुकीली चिबुक सहित हताश पुरुष का चेहरा जिसे उसकी दुःखी क्रुद्ध सहयोगिनी ढूँढ रही है और इसी प्रकार के अन्य चित्र इसके पश्चात् आता है अति-प्राकृत आकृतियों का क्रम ।
इस अवस्था में बनी उनकी चित्राकृतियाँ पर्याप्त विभ्रमात्मक है। रूप, रेखाएँ, कोण तथा रंग-सभी मानों खतरनाक हो गये हैं।
पृष्ठभूमियाँ हलचलपूर्ण है उदासी तथा भय का प्रतीक काला रंग प्रधान हो गया है और नरक में डूबी आकृतियाँ मानों बाहर झांकने लगी हैं; बड़े मुख-विवर, आँखें, उरोज, कान और आकृतियों के उल्टे पाँव (यह विश्वास किया जाता है कि भूतों के पाँच उल्टे अर्थात् पंजे पीछे की ओर तथा एडी आगे की ओर) होते हैं।
आकृतियों के रूप इतने विकृत कि उनके प्रति सम्पूर्ण आकर्षण समाप्त हो जाता है। पिशाचिनियों के शरीर विकृत, किन्तु मुख कोमल ।
इन प्रेतों के पश्चात् रवीन्द्रनाथ ठाकुर राक्षसाकृतियाँ चित्रित करने लगे । रवीन्द्रनाथ के इर्द-गिर्द बहुत समय तक गप्पी, शत्रु, मजाकिये और दुष्ट इकट्ठे रहे थे।
इन सबने उन्हें परेशान किया था किन्तु रवीन्द्रनाथ ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया इन राक्षस आकृतियों से उत्पन्न विषाद को कम करनेके लिए कुछ ऐसे पार्श्व चेहरे बनाने आरम्भ किये जो कथकलि अथवा सिंहली राक्षस मुखौटों से मिलते-जुलते है।
कोमल तथा गोल रूपों की लयात्मक अनुभूति के लिये रवीन्द्रनाथ ठाकुर नारीरूपों की ओर मुड़े ।
वे रूप जिनके आकर्षण पर उन्होंने अपनी युवावस्था में कोई ध्यान नहीं देना चाहा था, या निराशा के बावजूद भी उन्हें जो प्रिय थे ये नायिकाएँ रवीन्द्रनाथ के अतीत जीवन से चुराकर इन चित्रों में लायी गयी हैं।
इनकी मुखाकृतियाँ लिंगवत् लम्बाकार हैं। उनकी सहज दृष्टि और एकाकी चेहरे सूनापन लिये हैं तथा अपने पीछे छिपे सत्य को छिपाने का बहुत कम प्रयत्न करते हैं।
पर शायद इन चित्रों में चेहरों के आगे एक हल्की सुगन्धित समीर का भी आभास होता है।
नारी चेहरा अनेक रूप लेकर रवीन्द्र की कलाकृतियों में बार-बार प्रकट होता है। यह रवीन्द्र की प्रेमाश्रय स्थली और अभिलाषा की प्रतिमा है इसके सुखद स्पर्श को उन्होंने रंगों के प्रभावपूर्ण संगीत के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया है।
युवक रवीन्द्रनाथ ने स्वयं को भी चित्रित किया था। गोल चेहरे और मृदु दृष्टि वाला एक युवक जो भविष्य में झाँक रहा है। चित्र में सीपिया भूरे रंग का पतला वाश उनके स्वभाव के अनुरूप है।
किन्तु वृद्धावस्था में चित्रों में बनायी गयी स्वप्नाकृतियों में वे दूसरी बार युवा बने हैं, चित्रों से श्रृंगारिक सुख का अनुभव करते हुए ।
अन्तिम युग में उन्होंने दृश्य चित्र, मछलियों आदि का अंकन पर्याप्त तकनीकी कुशलता से किया है। किन्तु फिर उसे छोड़कर कभी-कभी रंगों के साथ क्रीड़ा भी की है।
रवीन्द्रनाथ की कला का विश्लेषण करते हुए डब्लू०जी० आर्चर ने कहा है कि फ्रायड तथा जुंग आदि ने मनोविश्लेषण का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है उसके अनुसार रवीन्द्रनाथ की चित्राकृतियाँ अचेतन से सम्बन्धित है तथा आधुनिक कला की स्वतः लेखन की विधि से बहुत मिलती-जुलती है।
आर्चर का यह भी विचार है कि रवीन्द्रनाथ की कला पर पाल क्ली का भी प्रभाव है। पाल क्ली ने भी अनेक चित्र अचेतन के प्रभाव में स्वतः लेखन अथवा स्वतः चित्रण की विधि से अंकित किये हैं।
दोनों ही रूप की अपेक्षा व्यंजना को प्रधान मनाते हैं। चित्र पहले बनता है, विषय का सम्बन्ध बाद में सोचा जाता है; और चित्र को शीर्षक सबसे अन्त में दिया जाता है।
रवीन्द्रनाथ पर अतियथार्थवादियों (पिकासो तथा डाली) के अतिरिक्त मोदिल्यानी तथा मुंक का भी प्रभाव देखा जा सकता है। विष्णु दे ने एमिल नोल्दे का प्रभाव भी इंगित किया गया है पर वास्तव में रवीन्द्रनाथ ने इन सभी समसामयिक आधुनिक यूरोपीय चित्रकारों की बहुत अधिक रचनाएँ नहीं देखी थीं।
इनकी तथा रवीन्द्रनाथ की कला में जो भी साम्य है वह केवल इसलिए है कि इन सबने लगभग एक-सी मनःस्थिति बनाकर चित्रांकन आरम्भ किया था। उन पर आदिम कला, लोक कला, बाल कला, वान गॉग, गॉगिन, एन्सर, आर्नुवो तथा नबी कला का भी प्रभाव माना जाता है।
गगनेन्द्रनाथ ठाकुर (1867-1938)
गगनेन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता में सन् 1867 ई० में हुआ था। इनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ के भतीजे थे अतः रवीन्द्रनाथ ठाकुर इनके चाचा लगते थे ।
गगनेन्द्रनाथ की बचपन से ही विभिन्न कलाओं में रूचि थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व का इन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। गगनेन्द्रनाथ ठाकुर प्रसिद्धि से दूर रहने वाले व्यक्ति थे अतः उन्होंने अपने जीवन का कोई वृतान्त नहीं छोड़ा है।
गगन बाबू के पिता का देहान्त तभी हो गया था जब गगन चौदह वर्ष के थे रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संरक्षण में इनका पालन-पोषण हुआ। आरम्भ में इन्होंने कला-विद्यालय की शिक्षण पद्धति पर आधारित जल-रंग चित्रण घर में ही सीखा।
इसके अतिरिक्त आरम्भ में इन्होंने पेंसिल से चित्रांकन भी सीखा। 1902-3 में जापानी चित्रकारों के इनके परिवार में ठहरने के कारण गगन बाबू ने भी जापानी चित्रांकन विधि सीख ली।
1910-15 में इन्होंने रवि बाबू की पुस्तक जीवन-स्मृति का चित्रण भी किया। इसके अतिरिक्त गगेन्द्रनाथ ने कुछ पर्वतीय दृश्य-चित्र भी बनाये आरम्भ में चौड़े तूलिकाघातों का प्रयोग किया किन्तु धीरे-धीरे ये तूलिकाघात छोटे होते गये हैं।
भारत में मौलिक विधि से विशुद्ध दृश्य चित्रण के आरम्भिक चित्रकार अवनीन्द्रनाथ तथा गगनेन्द्रनाथ ही माने जाते हैं।
इसके पश्चात् वाश शैली में चैतन्य चरित माला का चित्रण किया। चैतन्य के जन्म से देह त्याग तक के ये इक्कीस चित्र हैं जिनमें भाव-विभोर चैतन्य का संकीर्तनचित्र बहुत सुन्दर बन पड़ा है।
इनकी गतिपूर्ण आकृतियों तथा हल्के चमकदार रंग उस समय की पुनरुत्थान शैली से पर्याप्त भिन्न है। तीथों तथा रात्रि दृश्यों में काली स्याही अथवा गहरे रंगों द्वारा देवालयों के स्थापत्य, दर्शनार्थियों की भीड आदि का चित्रण किया है।
इनचित्रों में देवालयों के गर्भगृह से आता हुआ प्रकाश आध्यात्मिक धार्मिक प्रतीकता लिये हुएहै। धीरे-धीरे ये रात्रि के अन्धकार में अलोकिक शक्ति के प्रकाश से चमकते हुए देवालय चित्रित करने लगे।
यही पद्धति उन्होंने बाद में बनाये रहस्यमय भवनों के चित्रों में प्रयुक्त की है।
इस प्रकार के कुछ चित्रों में स्टेज-सेटिंग का भी प्रभाव है और धनवादी, भविष्यवादी तथा निर्माणवादी कला-आन्दोलनों की कल्पनाओं का उपयोग भी काली स्याही से अंकित इस प्रकार के चित्रों पर श्वेत-श्याम फोटोग्राफी का भी प्रभाव है।
सन् 1914 में पेरिस में भारतीय चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के भी छः चित्र थे।
इन चित्रों की पर्याप्त प्रशंसा हुई । 1921 से उन्होंने घनवादी शैली में प्रयोग आरम्भ किये और 1922 में डा० स्टैला क्रामरिश ने सर्व प्रथम उन्हें एक भारतीय घनवादी चित्रकार कहा।
सन् 1923 में बर्लिन में भारतीय आधुनिक चित्रकला की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें गगनेन्द्रनाथ की कृतियों को घनवादी कहा गया तथा यूरोपीय घनवादी कलाकारों से उनकी तुलना की गयी ।
उन्हें भारत का सबसे अधिक साहसी और आधुनिक चित्रकार माना गया। विनय कुमार सरकार ने उनका सम्बन्ध भविष्यवाद से जोड़ा। किन्तु वास्तव में गगनेन्द्रनाथ ठाकुर पूर्ण रूप से घनवादी अथवा भविष्यवादी चित्रकार नहीं हैं।
उनके चित्रों में अँधेरे अथवा प्रकाश वाले पारदर्शी तल एक दूसरे को कहीं बेधते हैं, कहीं आच्छादित कर लेते हैं। उनमें त्रिआयामी घनवादी ठोस रूपों के संयोजन अथवा प्रभाव नहीं है।
कोमल संवेदनाओं और छाया-प्रकाश के रहस्यात्मक प्रयोग के कारण वे रोमाण्टिक प्रतीत होते हैं उनके धनवाद में एक अतीन्द्रिय रहस्यात्मकता, समन्वयात्मक दृष्टि और आदर्शवादिता है जो उन्हें पश्चिमी धनवाद से पृथक करते हैं।
घनवादी आकृतियों के छोटे-छोटे रूपों के सघन जाल में भी वे कोई न कोई विषय ढूंढ ही लेते हैं।
जैसे हिमालय में वर्षा के दृश्य में अनेक समान्तर चतुर्भुजों की सृष्टि, बन्दिनी राजकुमारी के चित्र में अगणित त्रिभुज छाया-प्रकाश की क्रीडा करते अंकित हैं तथा नाचती लड़की के चित्र में सीढ़ियों, दालानों आदि के संयोजन में धुंधला प्रकाश इस तरह से अंकित है कि उससे आकृतियों, के एकदम अंधेरे वाले भाग स्पष्ट हो गये हैं।
घनवाद तथा प्रभाववाद के सर्वोत्तम तत्वों का समन्वय करके वे प्रधानतः प्रकाश का ही चित्रण करते हैं, चाहे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के जलते हुए लाल रंग बहुल चित्र हों चाहे अंधेरे में टिमटिमाती सड़क की रोशनी के ।
गगनेन्द्रनाथ ने रूपहले तथा सुनहरे धरातलों एवं रेशम पर काली स्याही से स्वच करके अनेक चित्र बनाये जिनमें कहीं-कहीं लाल तथा हरे रंगों के स्पर्श चित्रों को अपूर्व सौन्दर्य प्रदान करते हैं।
उनके प्रभाववादी चित्रों में कांग्रेस को सम्बोधित करते कवि रवीन्द्र, जंगल की आग, रायल जेकरिण्डा, बसन्त, राँची में सूर्यास्त आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।
उन्होंने अनेक नये और साहसपूर्ण प्रयोग भी किये। पुरी की स्वर्णिम रेत, तीर्थाटन तथा इसी प्रकार के अन्य चित्र सुनहरी धरातल पर स्याही से अंकित हैं जिनमें युक्तियों का बड़ा ही प्रभावी उपयोग हुआ है।
उन्होंने हिमालय के भी अनेक चित्र बनाये हैं। प्रकाश की प्रथम किरण इनमें सर्वश्रेष्ठ चित्र है जिसमें हिमालय के शिखर को हल्की गुलाबी तथा बैंगनी आभाओं से रंजित करती सूर्य की प्रथम रश्मियों का चित्रण किया गया है।
इसके पश्चात् उन्होंने जो चित्र बनाये उनमें प्रकाश का स्थान कम होने लगा और अंधेरे का भाग बढ़ने लगा।
यह अंधेरा एक रहस्यमय छायाकृति के रूप में चित्रित किया जाने लगा जो देखने में नारी जैसी है पर कहीं-कहीं उसके दाढ़ी भी चित्रित है। कहीं वह नासिका तथा मुख विवर को नकाब से ढके हुए है ।
गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन के अन्तिम चरण में काली स्याही से चौड़े तूलिकाघातों में पर्वतों तथा आकाश की ओर लपकते वृक्षों और उन पर उड़ते हुए मेघों का चित्रण किया।
सम्भवतः यह सब उनके मनकी बेचैनी की अभिव्यक्ति थी। अन्त में उन्हें पक्षाघात हो गया और 1938 में उनका देहावसान हो गया । उनकी कलात्मक प्रतिभा को भारतीय कला जगत् ही नहीं वरन् विदेशों में भी सराहा गया था।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब 1921 तथा 1926 में यूरोप गये थे तब कान्दिन्स्की, पाल क्ली तथा अन्य अभिव्यंजनावादी कलाकारों में उनकी लोकप्रियता देखकर आश्चर्य चकित रह गये थे।
गगनेन्द्रनाथ की कला को विषयानुसार निम्नप्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है-
1. परीलोक के समान वातावरण में रोमाण्टिक विषयों का चित्रण
2. काले तथा श्वेत रंगों में स्केच, व्यक्ति चित्र तथा सामाजिक व्यंग्य-विद्रूप
3. प्राकृतिक दृश्य
4. रहस्यपूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र
5. घनवादी चित्र
उनके व्यंग्यचित्र विकृतिपूर्ण नहीं है। वे सामाजिक स्थितियों पर व्यंग्य हैं। भारत में व्यंग्य चित्रण के आरम्भिक कलाकारों में से वे एक थे।
इस प्रकार गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने ठाकुर शैली तथा ठाकुर परिवार के मध्य रहकर भी स्वयं को उस तक सीमित नहीं रखा।
उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिये धनवादी शैली का प्रयोग किया तथा अन्य विदेशी शैलियों के समन्वय से अपनी कला का एक नितान्त मौलिक स्वरूप विकसित किया ।
बड़े साहस के साथ वे अपने मार्ग पर चले किन्तु उनकी पर्याप्त आलोचना भी हुई। उन्हें अभारतीय समझा गया और यह कहा गया कि यद्यपि कला में आदान-प्रदान होता है पर वह राष्ट्रीय भी होनी चाहिये।
उनके चित्रों में एक विचित्र माया-लोक के दर्शन होते हैं। उनकी कला को रोमाण्टिक यथार्थवादी कहा गया है। उनके कुछ चित्रों को स्वप्निल चित्रकला के अन्तर्गत भी रखा गया है ।
डिपार्चर आफ चैतन्य, द कमिंग आफ प्रिन्सेज, द फेयरी प्रिन्सेस, डेसोलेट हाउस, स्पिरिट आफ नाइट, सात भाई चम्पा, स्वप्न-जाल तथा द्वारका के मन्दिर आदि उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं।
यामिनी राय (1887-1972 ई०)
यामिनी रंजन राय का जन्म सन् 1887 ई० में बाँकुड़ा जिले के बेलियातोरे नामक गाँव में हुआ था। आपके पिता एक प्रतिष्ठित और सम्पन्न जमींदार थे किन्तु यामिनी राय गाँव के सभी वर्गों के लोगों से बे रोक-टोक मिलते थे।
बाँकुड़ा जिले की संस्कृति का बंगाल में एक विशिष्ट स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से यह बिहार की चट्टानी तथा गंगा की मैदानी भूमि की सम्मिलन स्थल है।
यहाँ से पश्चिम में संथाल, उत्तर में मल्ल तथा पूर्व में हिन्दू रहते हैं। बाँकुड़ा इन सभी का सम्मिलन स्थल है। इसमें बौद्ध, वैष्णव तथा शाक्त प्रभाव प्रमुख रहे हैं।
सर्प, नदी, शिव, शक्ति, मातृदेवियों आदि की पूजा की अनेक विधियाँ भी यहाँ प्रचलित हैं जो स्थानीय लोक विश्वासों तथा शास्त्रीय मान्यताओं का मिला-जुला रूप हैं।
इन्होंने यहाँ के निवासियों की सृजनशील कल्पना में बहुत योग दिया है। जीवन के विभिन्न पक्षों में आस्था और आशावाद यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है।
यामिनी राय पर इन सबका आरम्भ से ही प्रभाव पड़ा। यहाँ के समाजिक ढांचे में कलाकार और शिल्पी का कार्य एक ही व्यक्ति करता है और कला को निरुपयोगी नहीं समझा जाता।
गाँव में जो विभिन्न शिल्पी थे, यामिनी बाबू उनके सम्पर्क में आते गये। आस-पास के अन्य गाँवों में भ्रमण करके उन्होंने शिल्पों का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया।
मुख्यतः मिट्टी तथा काठ के खिलौनों तथा चित्रकारी के प्रति इनका झुकाव अधिक हो गया। जब गाँव में रास-लीला वालों की टोली आती तो बालक यामिनी उसके पीछे-पीछे घूमते ।
लोक शैली में चित्रांकन करने वाले पटुओं के प्रति उनमें अपार कुतूहल था।
खिलौने, गुड़िया, पूजा की मूर्तियाँ तथा पट चित्र बनाने वाले कुम्हार, बुनकर, बढई तथा देखा करते और उसमें प्रयुक्त अभिप्रायों तथा डिजाइनों की अनुकृति किया करते।
पटुओं के प्रति बालक यामिनी का आकर्षण बढ़ा। वे उनका काम एकटक वे इन कारीगरों से बहुत घुल-मिल गये थे।
परिवारी जनों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। धीरे-धीरे इनकी चित्रकला में रुचि बढ़ती गयी। बाँकुड़ा जिले की एक प्रदर्शनी में अपने चित्र “सोसाइटी” पर पुरस्कार प्राप्त करने से इनका उत्साह बढ़ गया।
जब ये सोलह वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनकी रुचि देखकर सन् 1903 में विदेशी पद्धति से कला की शिक्षा देने वाले कलकत्ता के गवर्नमेन्ट स्कूल आफ आर्ट में भेज दिया।
किन्तु इस विद्यालय में अन्य शिक्षा-संस्थाओं की ही भाँति एकेडेमिक पद्धति का बोलबाला था और समकालीन आन्दोलनों से उसका कोई वास्ता न था यामिनी राय ने वहाँ पर शास्त्रीय पद्धति से अनावृताओं का अंकन तथा तेल चित्र बनाना सीखा।
वे इसमें शीघ्र ही पारंगत हो गये और अध्ययन समाप्त करने के साथ ही कलकत्ता में एक उत्तम व्यावसायिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध भी हो गये।
जिस समय यामिनी राय यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसी अवधि में 1906 ई० में यहाँ भारतीय चित्रकला शिक्षण का विभाग भी स्थापित हुआ और अवनीन्द्रनाथ टैगोर उसके प्रभारी बने कलकत्ता कला विद्यालय छोड़ने के पश्चात् यामिनी राय को आजीविका की खोज में इलाहाबाद आना पड़ा।
इलाहाबाद तथा कुछ दिन पश्चात् कलकत्ता में उन्होंने लिथोग्राफी के छापाखानों में काम किया। फिर कुछ समय तक रंगीन ग्रीटिंग कार्ड्स बनाये।
कलकत्ता में ही उन्होंने काष्ठ मुद्रण के एक छापाखाने में कार्य किया। यहाँ कालीघाट पट-चित्र शैली की ही छपाई की एक विशिष्ट शैली विकसित हो गयी थी।
इसके पश्चात् उन्होंने यह सब छोड़कर तैल रंगों में यूरोपीय शैली के चित्र बनाना आरम्भ कर दिया।
इक्कीस वर्ष की आयु में 1908 में वे कलकत्ता में एक फैशनेबिल व्यक्ति चित्रकार के रूप में विख्यात हो गये।
वे व्यक्ति-चित्रों के साथ-साथ दृश्य चित्रों का अंकन भी करने लगे जो प्रभाववादी शैली में थे आलोचकों ने इन्हें बानगींग के दृश्य-चित्रों के समकक्ष माना है किन्तु पुरुषों को सामने बिठाकर और स्त्रियों के फोटोग्राफ द्वारा चित्र बनाते रहने पर शनः शनैः उन्हें घुटन प्रतीत होने लगी और वे अपने आप को अभिव्यक्त करने की विधियाँ ढूँढने लगे।
चित्रकारी के अतिरिक्त वे बंगाल के लोकनाट्य मंच से भी जुड़े रहे थे अतः उसकी यथार्थ लोक-भूमि ने भी उन पर प्रभाव छोड़ा था।
1921 ई० के लगभग उन्होंने अनुभव किया कि उनके लिए यूरोपीय शैली में आगे काम करना असंभव है।
उन्हें लगा कि आत्माभिव्यक्ति के लिए उस समाज की स्थापित परम्पराओं से जुडना आवश्यक है जिसके संस्कारों में वे पले हैं। इन्हीं सांस्कृतिक परम्पराओं में उन्हें अर्न्तदृष्टि तथा अनुभूति प्राप्त हो सकती है।
जिस प्रकार गोगिन, पिकासो तथा मातिरा ने आदिम कला, लोक-कला तथा पूर्वी कला-शैलियों से प्रेरणा ली थी उसी प्रकार यामिनी राय भी लोक-कला के मूल रूपों की खोज में लग गये।
उनका यह प्रयत्न केवल इच्छा या बुद्धि पर आधारित नहीं था बल्कि इसमें उन्होंने अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व झोंक दिया था।
इन प्रयोगों का महत्व उस समय नहीं समझा गया और यामिनी राय को यह समय अत्यधिक अर्थाभाव में व्यतीत करना पड़ा। अतः इस समय वे प्रायः रद्दी कागजों या आते आदि पर ही चित्रांकन करते रहे थे।
इसी अवधि में उनके युवा पुत्र की मृत्यू हो गयी; किन्तु इस आघात को सहन करते हुए भी उन्होंने प्रयत्न नहीं त्यागा।
उनकी प्रतिभा को कुछ विदेशियों ने पहचाना और 1930 ई० में “स्टेट्समैन” की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी के साथ यामिनी राय पुनः ख्याति की ओर बढ़ने लगे।
1929 से 1936 तक वे लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट में सहायक निर्देशक रहे। उसके पश्चात् दो वर्ष तक लाहौर के ही फोरमेन क्रिश्चियन कालेज के प्रधान शिक्षक रहे।
1938 से 1947 तक लाहौर के सिटी स्कूल आफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक के पद पर कार्य किया।
भारत विभाजन के पश्चात् वे दिल्ली चले आये जहाँ उन्होंने “शिल्पी चक्र” नामक संस्था का सूत्रपात किया। 1935 में कलकत्ता, 1946 तथा 1947 में लन्दन तथा 1953 में न्यूयार्क में उनके चित्रों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियाँ हुई।
उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार माना गया। 1955 में उन्हें भारत सरकार ने “पद्मभूषण” की उपाधि प्रदान कर उनकी कला का सम्मान किया।
1967 में उन्हें डी० लिट् की मानद उपाधि प्रदान की गयी। जीवन के अन्तिम क्षणों तक निरन्तर सृजन करते हुए 24 अप्रैल 1972 को उनका देहावसान हो गया।
यामिनी राय की कला
बाल्यकाल में यामिनी राय की कला पर बाँकुड़ा जिले की लोक-शैली का प्रभाव था। कलकत्ता में उन्होंने यूरापीय यथार्थवादी पद्धति तथा तैल माध्यम में कार्य किया साथ ही अनावृताओं का रेखांकन एवं प्रभाववादी शैली में दृश्यांकन किया।
यह सभी कार्य बहुत अच्छा बन पड़ा है। व्यक्ति चित्रण में तो वे इतने कुशल थे कि कलकत्ते में वे एक उत्तम शबीहकार (Portrait-Painter) के रूप में अल्प अवधि में ही विख्यात हो गये।
इसके पश्चात् उन पर कालीघाट की पट-चित्र शैली का प्रभाव पड़ा जिसमें सपाट भूरे अथवा सलेटी धरातलों पर काजल की गहरी तथा सशक्त रेखाओं द्वारा चित्रण किया जाता है।
“स्त्रियाँ” तथा “माँ और शिशु ” उनकी इसी समय की कृतियाँ हैं। सन् 1931 के पश्चात् उन्होंने कालीघाट के पट-चित्रो की शैली को त्याग कर बंगाल की लोक-कला के अन्य क्षेत्रों, बाँकुडा तथा हुगली से प्रेरणा लेना आरम्भ किया।
इनमें शुद्ध चमकदार रंगों तथा तीखी रेखाओं का अधिक प्रयोग है। यामिनी राय ने लोक-कला की रंग योजनाओं में कुछ नये रंगों को बढ़ा कर इन्हें और भी समृद्ध कर दिया है।
इस अवधि में उन्होंने रामायण तथा कृष्ण लीला का चित्रण किया है। इन चित्रों में एक चश्म चेहरे एक ही रेखा में माथे और नाक का अंकन, लाल पृष्ठिका तथा चमकदार शुद्ध रंगों की विशेषताऐं हैं; किन्तु रामायण के चित्रों की अधिक है।
तुलना में कृष्ण लीला के चित्रों में लयात्मकता तथा आलंकारिक प्रभाव पकाई मिट्टी के फलकों (Terracotta Tiles) से प्रेरणा ली है जिसकी भावभंगिमाओं, कृष्ण लीला के चित्रों में उन्होंने विष्णुपुर और वॉशावाटी के मन्दिरों की गढ़नशीलता तथा शक्तिमत्ता का यामिनी राय पर स्पष्ट प्रभाव है।
साथ ही उन पर बंगाल में 18वीं तथा 19वीं शती में चित्रित पाण्डुलिपियों के आवरण चित्रों की शैली का भी प्रभाव है।
लोक-कला के अन्य स्रोतों के रूप में उन्होंने बंगाल की अल्पना से पट आलंकारिकता और अमूर्तन, कन्था से सम्मुख आकृति योजना एवं लोक-जीवन, और खिलौनों तथा गुडियों से चमकीली रंग योजनाओं की प्रेरणा ली है।
उड़ीसा के चित्रों की छोटे-छोटे क्षेत्रों की संयोजन-पद्धति ने भी उन्हें प्रभावित किया है। कुछ चित्रों में अमरीकी प्राचीन ‘मय’ कला का भी प्रभाव लक्षित होता है।
1937 में उन्होंने ईसा के जीवन पर चित्र बनाना आरम्भ किया। जब उनसे इस विषय में पूछा गया कि आप स्वयं ईसाई नहीं हैं, न ही आपने बाइबिल पढ़ी है और एक विदेशी विषय को आप कैसे आत्मसात् कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि वे ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो नया तकनीक विकसित किया है वह इस प्रकार के विषय को सफलतापूर्वक अंकित कर सकता है अथवा नहीं जो उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित नहीं हैं।
इसके लिए उन्हें ईसा का जीवन बहुत उपयुक्त प्रतीत हुआ। वे ईसा की मानवता वादी भावना को प्रदर्शित करने में रिनेसाँ के यथार्थवादी अथवा प्राकृतिकतावादी कलाकारों की कृतियों से संतुष्ट नहीं थे और यह दिखाना चाहते थे कि केवल अमूर्त और प्रतीक विधि से ही ईसाई मानव और देवता के एकत्व की भावना प्रकट की जा सकती है।
इसमें सन्देह नहीं कि जो आत्मीयता और कोमलता यामिनी राय के ईसा-विषयक चित्रों में है वह न तो बाइजेण्टाइन कला में है, न प्राकृतिकतावादी कला में उसका कुछ अनुभव रूसी लोक-कला की प्रतिमाओं (ICONS) में अवश्य किया जा सकता है।
1940 के उपरान्त कालीघाट के पट-चित्रों की पद्धति पर उन्होंने बिल्लियों की विभिन्न स्थितियों के चित्र बनाये हैं जो उनके तूलिका पर सशक्त अधिकार के साथ-साथ तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर भी व्यंग्य भी हैं।
यामिनी राय ने धरातलीय वयन (टेक्सचर) के सम्बन्ध में भी प्रयोग किये। वे सपाट चिकना धरातल बनाने के बजाय उसे कागज की पट्टियों को चटाई की भाँति बुनकर खुरदुरा बनाने लगे।
उन्होंने कागज, गत्ता, कपड़ा तथा बर्तनों पर भी चित्रकारी की है और जल रंगों, क्रेयन तथा टेम्परा से ही अधिकांश कार्य किया है।
यामिनी राय ने न तो पश्चिमी बंगाल की थोथी अनुकृति की है और न भारत की लुप्त प्रायः परम्पराओं का निर्जीव अनुकरण ही किया है।
उनकी कला में न विदेशीपन है, न ठाकुर शैली की धूमिल नैराश्य भावना। बंगाल की लोक-कला के अनुशीलन से उन्होंने एक सर्वथा मौलिक शैली की उद्भावना की है।
आलोचकों के अनुसार उनके प्रतीकों में मौलिकता नहीं है। यह ठीक है, किन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि लोक-जीवन में व्याप्त उनके प्रतीक चिर-नूतन हैं।
उन्होंने उन्हें नई व्यवस्था और नव-जीवन दिया है। उन्हें पुष्ट बनाया है और दी है सार्वभौमिकता, जिसके बिना ये प्रतीक बंगाल की परिधि से बाहर नहीं निकल पाते।
दूसरी आलोचना उनके विषय में यह की जाती है कि उन्होंने स्वयं को निरन्तर दुहराया है। वास्तव में यामिनी राय ने कुछ मूल तत्वों को सरलीकृत कर लिया था और उन्हीं को वे सदैव प्रयुक्त करते रहे हैं।
इसी से देखने वालों को उनमें एकरसता अथवा पुनरावृत्ति-सी होती प्रतीत होती है।
यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा जाता है; किन्तु यह अतिशयोक्ति है।
इसमें संदेह नहीं हैं कि पिकासो की भाँति वे भी अपने शिल्प में पूर्ण दक्ष थे, किन्तु पिकासो एक सच्चे कलाकार की तरह जहाँ नयी-नयी खोजों में लगा रहा वहाँ यामिनी राय एक ही शैली के विकास में लगे रहे।
कल्पनाशील कलाकार किसी एक ही शैली में बंधकर जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि यामिनी बाबू ने भी पश्चिमी शैली, वान गॉग की पद्धति, ठाकुर शैली एवं लोक शैली का क्रमशः अभ्यास किया था तथापि वे पिकासो की भाँति आधुनिक कला के महान अग्रदूत नहीं बन पाये।
आज की शैलियाँ लोक-कला एवं आदिम कला के धरातल पर ही परस्पर निकट आ सकती हैं, उन्होंने इसे समझ लिया था; किन्तु उनकी कला में आधुनिक जीवन की चेतना का अभाव है।
यूरोपीय कला समीक्षकों ने यामिनी राय की ईसाई धर्म विषयक कृतियों और रूसी-बाइजेंटाइन कला-कृतियों में अद्भुत तत्व-साम्य का अनुभव किया है और यह स्वीकारा है कि यामिनी बाबू की कला में निश्चय ही मौलिकता और उच्च भावभूमि है।
आकृति-चित्रण की सरलता के कारण उनकी तुलना आधुनिक चित्रकार हेनरी मातिस से भी की जाती है। यामिनी राय से प्रेरित होकर अनेक नये कलाकार लोक-शैलियों की ओर उन्मुख हुए हैं।
जार्ज कीट (1901) जार्ज कीट जन्म से सिंहली किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय हैं । उनका जन्म श्रीलंका के केण्डी नामक स्थान पर 17 अप्रैल सन् 1901 को हुआ था।
उनके पिता भारतीय मूल के और माता डच परिवार की थीं। उनका पालन-पोषण पाश्चात्य सभ्यता में ढले उच्च वर्गीय वातावरण में हुआ था। बाल्यावस्था से ही जार्ज को चित्र बनाने तथा नये-नये आविष्कारों का शौक था।
दस वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ना आरम्भ किया। अंग्रेजी साहित्य के अनुशीलन से उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ; साथ ही वे चित्रांकन में भी रूचि लेते रहे ।
उच्च शिक्षा के के कारण उन्होंने 1918 में पढ़ाई छोड़ दी। 1918 से 1927 तक उन्होंने हिन्दू तथा लिए उन्होंने केण्डी के ट्रिनिटी कालेज में प्रवेश लिया किन्तु कला में विशेष अभिरूचि बौद्ध धर्म, कला और साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया ।
इससे उनका भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ा । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की लंका यात्रा के समय वे उनके व्याख्यानों से अत्यधिक प्रभावित हुए और शान्ति निकेतन जाकर पढ़ने की इच्छा प्रकट की किन्तु घर वालों ने उनकी इस बात का मजाक बनाया और कला की शिक्षा के लिये इंग्लण्ड जानेका परामर्श दिया।
इसके पश्चात् उन्होंने सिंहली धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया। उन्होंने सिहली, पाली और संस्कृत भाषाएँ भी सीखी।
इससे उनके व्यक्ति तथा कला पर हिन्दू एवं बौद्ध धर्म तथा दर्शन का प्रभाव पड़ा। 1920 के पश्चात् उन्होंन बौद्ध पत्र-पत्रिकाओं के लिये अगले चालीस वर्ष तक अनेक लेख लिखे और चित्र बनाये
सन् 1926 से वे चित्रकला में विशेष रूप से दत्त-चित्त रहने लगे। उन्होंने लंका में कुछ यूरोपीय कला शिक्षकों से तकनीकी शिक्षा भी ग्रहण की। 1928 में वे सीलोन आर्ट क्लब के सदस्य बने ।
साथ ही भारतीय कला परम्पराओं तथा सिंहली लोक कला का भी अध्ययन किया । 1928 में उन्होंने गोविन्दम्मा नामक नर्तकी को माडल कई बनाकर अनावृत चित्र अंकित किया।
इसके पश्चात् उन्होंने अनावृत नारियों के क चित्र बनाये । इसी समय जार्ज कीट ने कृष्ण तथा गोपियों के विषय का चित्रांकन प्रारम्भ किया।
1928-30 के मध्य उन्होंने कैण्डी तथा आस-पास के क्षेत्र के कई दृश्य चित्रित किये, साथ ही सिंहली जन-जीवन के भी कुछ चित्रों का अंकन किया इन पर सेजान और पाल गॉगिंग का स्पष्ट प्रभाव है।
जार्ज कीट द्वारा बनाये गये विधा जीवन के चित्र पिकासो से मिलते-जुलते हैं। 1928 की एक प्रदर्शनी में उन्होंने नार लिया।
वहाँ उन्हें नव-भविष्यवादी कलाकार कहा गया । 1929 में उन्होंने पुनः एक प्रदर्शनी में श्रीलंका के कई प्रसिद्ध चित्रकारों के साथ भाग लिया।
जनवरी 1930 में उन्होंने जब तीसरी बार अपने चित्र प्रदर्शित किये तो उन्हें बहुत प्रशंसा मिली मिली। यहीं से जार्ज कीट को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिलनी आरम्भ हुई ।
1930 तथा 1932 के मध्य उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का चित्रण किया। ये चित्र अत्यन्त संयत शैली में बनाये गये हैं तथा कृष्ण-राधा से सम्बन्धित पूर्व-रचित चित्रों से पर्याप्त भिन्न हैं।
इसी युग के अनावृताओं के चित्रों के शरीर के ठोस आय का चित्रण पिकासो के समान है।
सन् 1933 से जार्ज कीट की कला में अमूर्त रूपों एवं रेखाओं का आधिक्य ह लगा इस समय के उनके रूप संश्लेषात्मक धनवाद (सिन्थेटिक क्यूबिज्म) के निकट हैं।
इनमें दो चेहरों को एक कर देने वाली शैली पिकासो की है जिसे जार्ज की ने भारतीय अद्वैत दर्शन के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। 1936 से जार्ज कीट ने हिर पौराणिक आख्यानों तथा काव्यों के आधार पर चित्रण प्रारम्भ किया।
इनमें जयदे कृत गीत गोविन्द पर आधारित कृष्ण-राधा की प्रणय-लीला का विषय प्रमुख है। 1937 में चित्रित ‘वर्षा-विहार’ इस क्रम की सर्वश्रेष्ठ कृति है।
इस समय जार्ज क के जीवन में जो विपत्तियों आयीं उनके कारण उन्होंने संयोग श्रृंगार के तुरन्त विरह के चित्र बनाये। इसी अवधि में विरह से सम्बन्धित उनके दो कविता-संग्रह सन प्रकाशित हुए ।
भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन और द्वितीय विश्वयुद्ध की आशंका से उनके चित्रों में विशेष विकृति और तनाव भी आ गया है। इसके पश्चात् उनके चित्रों में यह तनाव कम हो गया।
उन्होंने कोलम्बों के गौतमी बिहार में गौतम बुद्ध का जीवन चित्रित किया। 1939 में उन्होंने दक्षिण भारत के मदुरै, श्रीरंगम् और चिदम्बरम् नामक स्थानों की यात्रा की तथा भारत के विविध नृत्यों के कार्यक्रमों से प्रभावित हुए ।
यहाँ से वापस लौटकर उन्होंने गौतमी विहार के चित्र पूर्ण किये। ये सभी चित्र तैल माध्यम में बने हैं और जार्ज कीट की शैली की शक्तिमत्ता के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनमें भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का सुन्दर समन्वय भी हुआ है।
1940 से 1946 ई० तक जार्ज कीट ने चित्रण से लगभग सन्यास ले लिया और एकान्तवास में रहे केवल कुछ चित्र भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन से प्रेरित होकर अवश्य अंकित किये।
इस समय की उनकी कृति “भीम और जरासन्ध” संसार की फासिस्ट शक्तियों की प्रतीक है।
1946 के पश्चात् पुनः श्रृंगार विषयक “नायिका” चित्रों का क्रम आरम्भ हुआ। 1943 में श्रीलंका में “ग्रुप 43” की स्थापना हो चुकी थी और जार्ज कीट इसके संस्थापक सदस्य थे।
1946 के अन्त में वे पुनः भारत आये। यहाँ उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगायी गयी। यहीं पर उनका परिचय कुसुम नामक युवती से हुआ जो उनसे टेम्परा चित्रण विधि सीखना चाहती थीं।
बाद में यह परिचय प्रणय बन्धन में परिवर्तित हो गया। सम्भवतः कीट की 1946 के पश्चात् की कला में श्रृंगारिक विषयों का पुनः प्रवेश उनके व्यक्तिगत जीवन के इस मधुर प्रसंग के कारण ही हुआ है।
स्वयं जार्ज कीट का कथन है कि कुसुम के संसर्ग के आनन्द से ही मेरी नायिकाओं का गुलाबी मॉसल वर्ण हो गया है।
जार्ज कीट के परवर्ती जीवन में चित्रों की प्रेरणा हिन्दू तथा बौद्ध कथाएँ रही हैं।
उन्होंने जातक कथाओं, नायिका, राग-रागिनी, कृष्ण लीला एवं श्रीलंका के जन-जीवन तथा प्रकृति से सम्बन्धित चित्रों का अंकन किया है।
उनके गीत-गोविन्द के चित्र विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी कला पर सेजान, गोंगिन तथा पिकासो के अतिरिक्त अजन्ता, सिगिरिय, चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं, केण्डी की लोक कला, दक्षिणी भित्ति चित्रों तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव है।
सेजान से उन्होंने वस्तुओं के ढाँचे को समझा है, गॉगिन से उन्होंने रंग की ऐन्द्रिक अनुभूति ली है, अजन्ता तथा सिगिरिय से रेखा का शास्त्रीय माधुर्य सीखा है, दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमाओं से लय तथा गतिमय ओज का अनुभव प्राप्त किया है, लोक कला से स्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति अपनाई है तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर से सहजता का गुण प्राप्त किया है।
कीट के संयोजनों की शक्ति मुख्यतः रेखाओं पर निर्भर है जो आवश्यकतानुसार दृढ़, मोटी, शिथिल अथवा बारीक हैं, किन्तु दुर्बल अथवा अनिश्चित नहीं ।
अमृता शेरगिल (1913-1941 ई०)
अमृता शेरगिल के पिता उमराव सिंह शेरगिल पंजाब में अमृतसर के निकट मजीठा तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट सरैया गाँव के जागीरदार थे।
उनकी माता मारिया आन्त्वानेत हंगेरियन थीं। युवती मारिया जब भारत भ्रमण के लिए आयी हुई थीं तो पंजाब में उनकी भेंट उमरावसिंह से हुई और दोनों प्रणय सूत्र में बंध गये।
उमरावसिंह अनेक भाषाओं के विज्ञान, तत्वज्ञानी तथा धार्मिक व्यक्ति थे। माता संगीत प्रेमी महिला थीं। इन्हीं के परिवार में अमृता का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुदापेरत में हुआ था।
अमृता का बचपन हंगरी में ही व्यतीत हुआ और उन्हें बचपन से ही अपनी प्रतिभा के विकास का पूरा अवसर मिला। चित्रकला में भी उनकी आरम्भ से ही रुचि थी।
जब ये साढ़े पांच वर्ष की थी, तभी रंगीन पाक से अपने आस-पास के खिलौनों के चित्र बनाना आरम्भ कर दिया था। सात वर्ष की आयु में उन्होंने हंगरी की परी कहानियों तथा बालकों की वेश-भूषा के सुन्दर चित्र बनाये थे आठ वर्ष की आयु में वे प्रथम बार भारत आय।
तब तक प्रथम महायुद्ध समाप्त हो चुका था। उनके साथ माता-पिता के अतिरिक्त छोटी बहिन इन्दिरा भी थी। मार्ग में पेरिस में उन्होंने खूब संग्रहालय देखा जहां विश्व-विख्यात यूरोपीय कलाकारों के अनेक चित्र तथा लियोनार्दो की ‘मोनालिसा’ भी है।
यहां होते हुए वे बम्बई उतरी और कुछ दिन बम्बई तथा दिल्ली में रहीं। इसके पश्चात् वे अपने पैतृक निवास स्थान समर हिल शिमला चली गयीं।
वहां उनकी शिक्षा रईसी ढंग से हुई। उनके लिए बारी-बारी से कई कला शिक्षक भी नियुक्त किये गये।
सन् 1924 में ग्यारह वर्ष की आयु में अमृता को इटली के फ्लोरेन्स नगर के कला-विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया किन्तु वहां की शिक्षण-पद्धति अमृता के अनुकूल नहीं थी अतः वे भारत लौट आयीं और 1924 से 1927 तक घर पर ही कला का अभ्यास करती रहीं।
इस अवधि में उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया उसके कारण उनके परिवार के शुभ-चिन्तकों ने उन्हें पुनः यूरोप जाकर कला के अध्ययन का परामर्श दिया।
1929 में वे पुनः पेरिस पहुँची। वहाँ कुछ समय तक अन्य कला शिक्षकों के सम्पर्क में रहने के उपरान्त अन्त में 1929 से 1934 तक पाँच वर्ष तक उन्होंने वहाँ के प्रसिद्ध कला-शिक्षक लूसियों साइमों के निर्देशन में “इकोल द बुआज आर्त’ में कला की शिक्षा प्राप्त की।
1930 ई० के लगभग उन्होंने तैल चित्रण आरम्भ किया। इसी बीच तीन महीने के लिए वे हंगरी भी गयीं। पेरिस में वे प्रतिवर्ष अपने चित्रों की प्रर्दशनी भी करती रहती थीं।
वे स्वभाव से नास्तिक थीं और यूरोपीय वातावरण का उनपर प्रबल प्रभाव था। वे परिस की बोहीमियन जिन्दगी के भी निकट सम्पर्क में आय र्थी अतः उनका जीवन बहुत उन्मुक्त था और वे बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। तीन वर्ष के पश्चात् उन्होंने सन् 1932 में ग्रांद सेलून में जो चित्र प्रदर्शित किये उनमें ‘युवा कन्याऐं’ शीर्षक चित्र की मुक्त से प्रशंसा की गयी।
यह चित्र यद्यपि कला विद्यालय की शिक्षा स्तर का है तथापि इस कंठ पर सेजान का भी प्रभाव है किन्तु यूरोप में चित्रकला के क्षेत्र में पुरस्कार एवं यश प्राप्त करने के उपरान्त भी उन्हें ये अनुभव हुआ कि वे यूरोप में पिकासो अथवा माति जैसे कलाकारों की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकतीं।
उनके मन में यह धारणा बैठ गई कि उनका कार्य क्षेत्र भारत ही हो सकता है। 1934 ई० में वे अपने माता-पिता के साथ भारत लीटी और मजीठा (पंजाब) तथा सरैया (गोरखपुर, उ० प्र०) होती हुई शिमला में रहने लगीं और चित्रण में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करने लगीं।
यूरोप में वे नग्न मॉडल बैठाकर चित्रण किया करती थी, उसी विधि से भारत आने घर भी उन्होंने परिवार, मित्रों तथा घरेलू नौकरानियों आदि के चित्र अंकित किये।
सन् 1935 में अमृता ने फाइन आर्ट्स सोसाइटी को अपने कुछ चित्र प्रदर्शनी के लिए भेजे। सोसाइटी ने जो चित्र लौटाये उनमें एक चित्र वह भी था जिस पर उन्हें पेरिस में पुरस्कार मिल चुका था।
इससे अमृता को गहरी ठेस लगी और उन्होंने सोसाइटी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार भी वापिस कर दिया। भारत में रहकर अमृता ने जो चित्र बनाये उनमें आकृतियों के सरलीकरण के साथ-साथ यहाँ के जन-साधारण की मार्मिक परिस्थितियों को भी कुशलता से चित्रित किया गया है।
इनमें बाल-बधू, भारतीय माँ, भिक्षुक, तीन कन्याएँ तथा पर्वतीय महिलाऐं आदि प्रमुख हैं।
1936 में वे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते समय बम्बई में कार्ल खण्डालावाला से मिलीं। वहाँ अमृता को प्रशंसा भी मिली और उनके संग्रह में अनेक उत्तम कोटि के भारतीय लघु चित्र भी देखने को मिले।
बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय में भी उन्होंने चित्रों का अध्ययन किया। राजस्थानी तथा बसौली शैली के चित्रों के अ ययन का उन्होंने बाद में बनाये चित्रों में उपयोग किया।
बम्बई में उन्होंने ताजमहल होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी की। अजन्ता तथा एलोरा उन्हें बहुत अच्छे लगे। अजन्ता के विषय में उन्होंने कहा था कि “अजन्ता ! वह तो मेरी समझ से बाहर की चीज है”।
अमृता ने दक्षिण में कोचीन, त्रिवेन्द्रम, कन्याकुमारी, मदुरै तथा मत्तनचारी के मन्दिरों के भित्ति चित्रों, दक्षिणी भूमि, वनस्पति और वहाँ के अर्द्ध नग्न नर-नारियों को देखा और उन सबका उनकी कला में भी प्रभाव आया।
1936 में ही अमृता ने अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ हैदराबाद, इलाहाबाद तथा दिल्ली में आयोजित कीं। दिल्ली प्रदर्शनी के समय उनकी भेंट जवाहरलाल नेहरू से भी हुई।
1937 में अमृता ने अपने चुने हुए तीस चित्रों की प्रदर्शनी लाहौर में की। इससे उनकी बहुत ख्याति हुई और अनेक समाचार पत्रों ने उनकी प्रशंसा की।
इसी समय ये हडप्पा के अवशेष देखने भी गई। कुछ समय पश्चात् वे सरैया चली गयीं। 1938 में उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें उन्हें अपने दो आत्म-चित्रों पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
1938 में अमृता ने अपने हंगरी के रिश्ते में चचेरे भाई विक्टर एगान से विवाह किया जो एक सैनिक थे। वे एक वर्ष तक वहीं रही और छोटी-छोटी जगहों पर घूमती रहीं।
इस समय उन्होंने सरल शैली में “हंगरी का हाट” आदि चित्रों की रचना की। इसी समय महायुद्ध की आशंका होने के कारण वे अपने पति के साथ 1939 ई० में श्रीलंका, महाबलीपुरम तथा मथुरा होते हुए शिमला लौटी। मथुरा की कला के प्रति ये बहुत आकर्षित हुई।
मथुरा से शिमला पहुँचने के कुछ समय पश्चात् विक्टर एगान के साथ सरैया पहुँचीं। यहाँ उन्होंने भारतीय नारी की घरेलू, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने और चित्रित करने का प्रयत्न किया।
इस समय के उनके चित्रों में ‘झूला’, कहानी कहने वाला, वधू, चारपाई पर विश्राम करती महिला आदि प्रमुख हैं। 1940 में अमृता को बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा पुरस्कृत किया गया।
1941 में अमृता लाहौर चली आयीं जहाँ उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आकाशवाणी-वार्ताओं आदि में भाग लेना आरम्भ कर दिया।
अमृता का स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा रहा था और 5 दिसम्बर 1941 को केवल 29 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया।
अमृता की कला- अमृता की आरम्भ से ही मानव शरीर के चित्रण में विशेष रुचि थी। जब वे बालक थीं तभी सुन्दर वेशधारी बच्चों के रेखाचित्र रंगीन चाक आदि से बनाती थीं।
उनके आरम्भिक शिक्षकों ने उन्हें यूरोपीय पद्धति से माडल बिठाकर चित्रांकन करने को प्रेरित किया। पहले तो उन्होंने जल रंगों से कार्य किया किन्तु शीघ्र ही वे तैल माध्यम में कार्य करने लग गईं।
किशोरावस्था में ही वे यूरोप के कलाकारों की भाँति नग्न- मानव-माडल बिठाकर चित्रांकन करने लगी थीं। इसमें उन्होंने जो तकनीकी कुशलता तथा शारीरिक सौन्दर्य के चित्रण में दक्षता प्राप्त की थी उसका प्रभाव “स्त्री की पीठ” के चित्र में देखा जाता है।
उनके द्वारा अंकित कोयले से बनाये गये स्केचों तथा अध्ययन चित्रों में रेखाओं तथा बलों का अच्छा योग है। यूरोपीय प्रवास के समय उन पर गॉगिन, वान गॉग तथा सेजान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जिससे उनकी कलाकृतियों में सरलता का समावेश हुआ।
1936 से उन पर भारतीय लघु चित्रों के रंगों के सौन्दर्य का भी प्रभाव पड़ा जो अन्त तक दिखायी देता है। 1938 में जब वे विक्टर एगान से विवाह करने पुनः हंगरी गयीं तो ब्रूगेल द एल्डर की सरल रंग-योजनाओं से भी प्रभावित हुई और इसी प्रभाव में उन्होंने हंगरी के बाजार का दृश्य बनाया। इस समय के चित्रों में छाया और सादगी का एक विचित्र संयोग है।
दक्षिण भारत भ्रमण के पश्चात् अमृता ने दक्षिण में किये गये स्केचों के आधार पर जो चित्र बनाये उनके लिए शिमला के लोगों को माडल बनाया।
इससे इन चित्रों में वास्तविकता का अभाव आ गया है। रंग-योजनाएँ तथा मुद्राएँ यद्यपि व्यंजक हैं तथापि मुखाकृतियाँ मार्मिक और स्वाभाविक नहीं हैं।
अमृता की कला में पूर्व और पश्चिम की शैलियों का समन्वय हुआ है। उन्होंने यूरोपकी आधुनिक आकृति-मूलक शैलियों के साथ भारतीय लघु चित्र शैलियों का समन्वय किया है।
उनकी आकृतियों में गॉगिन के समान आदिम सरलता, सेजान के समान गढ़न का प्रभाव, भारतीय लघु चित्रों के समान वर्ण-सौन्दर्य, ब्रूगेल द एल्डर के समान सपाट छाया वाले स्थानों का चित्रण तथा अभिव्यंजनावादियों के समान रूपों और रंगों की अनुभूति है।
उन्होंने आकृतियों को सरल बनाया और उन्हें गहरी बुझी रेखाओं से घेरा । यद्यपि उन्होंने कुछ प्राकृतिक दृश्यों, हाट तथा व्यक्ति-चित्रों का भी अंकनकिया है पर उनकी कला में भारतीय जन-जीवन के समाजिक पक्ष, विशेष रूप से नारी के जीवन का भी पर्याप्त चित्रण है। लाल रंग उनका प्रिय रंग है जिसके अनेक बलों का उन्होंने प्रयोग किया है।
यह हंगरी के लोक-जीवन में तो व्याप्त है ही, अमृता के भोग-विलासपूर्ण जीवन का भी द्योतक है।
अमृता ने यद्यपि तैल माध्यम का प्रयोग किया है किन्तु उनके चित्र टेम्परा में अंकित भित्ति चित्रों जैसे लगते हैं ।
अमृता शेरगिल की ख्याति मुख्यतः पाँच चित्रों पर आधारित है 1. पर्वतीय पुरुष, 2. पर्वतीय स्त्रियों 3. ब्रह्मचारी, 4. वधू का श्रृंगार तथा 5. बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण इसके साथ एक चित्र और जोड़ दिया जाता है फल बेचने वाले – (या केले बेचने वाले) ।
पर्वतीय स्त्री-पुरुषों के चित्र में लोग पास-पास खड़े अवश्य हैं पर उनमें परस्पर आत्मीयता का पूर्ण अभाव है। शायद यह उनलोगों के जीवन की वास्तविक दूरियों को प्रकट करता है।
वधू का श्रृंगार तथा ब्रहमचारी में अजन्ताकी प्रेरणा से अंगों की लम्बाई और मुद्राएँ प्रभावित हैं। इन दोनों चित्रों में भी पुरूषों तथा स्त्रियों के समूह पृथक् ही चित्रित किये गये हैं। साथ ही फ्रेंच अकादमी का भी प्रभाव है।
सम्भवतः एक चीनी मिल के मालिक पूँजीपति की पुत्री होने के कारण उनके दृष्टिकोण में सहानुभूति नहीं झलकती। उन्होंने भारतीय जन-जीवन के भावुकतापूर्ण चित्र ही अंकित किये जैसे मदर इण्डिया, भिखारी, स्त्री, सूरजमुखी आदि। उनके भावुकतापूर्ण मन को भारत की गरीबी सुन्दर लगती थी।
भारतीयों की दयनीय अवस्था उनके लिये केवल एक उत्तेजना मात्र थी। उन्होंने लिखा भी है कि यदि “भारत में गरीब न होते तो मेरे लिये पेण्ट करने को कुछ भी नहीं होता।”
तकनीकी दृष्टि से यूरोपीय कला-शिक्षा पर गर्व होते हुए भी उन्हें अपना भविष्य यूरोप में न दिखाई देकर भारत में ही दिखाई देता था।
फिर भी अपनी शैली के मौलिक विकास में उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। यदि वे जीवित रहती तो उनकी कला में भी विकास होता ।
अमृता शेरगिल ने पाश्चात्य अंकन पद्धति तथा भारतीय जीवन-दृष्टि को अपनी कला का आधार बनाया । आकृतियाँ सुनिश्चित और उच्च कोटि की रंग योजनाएँ उनके चित्रों की मुख्य विशेषताएँ हैं।
अमृता शेरगिल हमारे सामने उस समय आर्यी थी जब ठाकुर शैली की मौलिक प्रेरणा का हास हो गया था। कलाकारों का अधिकांश वर्ग अतीत में ही उलझा हुआ था और कला सम्बन्धी विचारों में एक अजीब अस्पष्टता फैली हुई थी।
उन्होंने इस काई को काटने का यत्न किया और भारतीय कला को नया मूल्य दिया । उनके प्रयोगों ने नये चित्रकारों को नये प्रयोग करने की उमंग दी यह अमृता की ऐतिहासिक देव थी। भारत की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में उनका नाम नींव के पत्थरों में गिना जाता है।
अपनी कला, स्वभाव, चरित्र तथा व्यक्तित्व में अमृता निवासी कवि बायरन का भारतीय नारी-संस्करण कहा गया है।
विदेशी कलाकार
निकोलस रोरिक (1874-1947) सुदूर के देशों से आकर भारतीय प्रकृति, दर्शन और संस्कृति से प्रभावित होकर यहीं पर बस जाने वाले महापुरूषों में रूसी कलाकार निकोलस रोरिक का नाम शीर्ष स्थान पर है।
उनका दृष्टिकोण विश्वजनीन था किन्तु भारत में हिमालय के क्षेत्र में ही उनको आत्मिक शान्ति का अनुभव हुआ था। यहाँ रहकर वे भारतीय संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़ गये थे।
निकोलस रोरिक का जन्म 1874 ई० में सेण्ट पीटसबर्ग में एक वकील के घर में हुआ था। बचपन से ही उनकी रूचि इतिहास तथा कलामें थी।
उन्होंने सेण्ट पीटसवर्ग विश्व विद्यालय से वकालत की डिग्री के साथ-साथ ललित कला अकादमी की स्नातक उपाधि भी प्राप्त की जहाँ पर उन्होंने प्रसिद्ध रूसी दृश्य चित्रकार आर्खिप कुइन जी से चित्र विद्या सीखी थी।
इसके उपरान्त रोरिक ने स्वयं को चित्रकला के प्रति समर्पित कर दिया। इस कार्य में रूसी संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान ब्लादिमीर स्तासोव ने उन्हें प्रोत्साहित किया और रूसी सांस्कृतिक इतिहास के अनुशीलन का परामर्श दिया।
इसके आधार पर रोरिक ने रूसी जन-जीवन के संघर्षमय इतिहास को काल्पनिक कथा (मिथक) के समान चित्रित करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने इतिहास की वास्तविक घटनाओं के अंकन में रूचि नहीं ली।
अपने चित्रों के लिए उन्होंने बलिष्ठ नर नारियों, विशाल तथा भारी नौकाओं, पर्वतों तथा घाटियों का ऐसा लोक सर्जित किया जहाँ प्रत्येक वस्तु ठोस तथा शक्तिशाली है, स्पष्ट और स्थायित्वपूर्ण है रोरिक ने प्राचीन युग को ऐसी भव्यता भी दी जो वर्तमान में नहीं है।
उन्होंने इतिहास की अनुभूति के लिए रूस के प्राचीन नगरों की यात्राएँ भी की। 1903-4 में उन्होंने प्राचीन पूजागृहों, मीनारों तथा नगरों को घेरने वाली प्रकोष्ठ दीवारों के अस्सी से भी अधिक चित्र बनाये ।
रूस ही नहीं, रोरिक को प्राचीन तथा मध्यकालीन पूर्वी संस्कृति, मध्य-युगीन यूरोपीय संस्कृति तथा स्क्रेडिनेवियन कला से भी प्रेम था। उन्होंने इनके विषय में अनेक लेख लिखे थे। उनके लिखे 27 ग्रंथ उपलब्ध हैं।
रोरिक ने बड़े आकार के आलंकारिक भित्ति चित्रों, पेनल चित्रों तथा मणिकुट्टिम चित्रों की भी रचना की । अपने युग के महान् वास्तुकारों के साथ उन्होंने भवन तथा चित्रकला के समन्वय की समस्या पर भी प्रयोग किये और आधुनिक भवनों में प्रयोग के लिये मणिकुट्टिम, चिलिचित्र तथा पेनल-चित्र बनाये।
1910 में उन्होंने पीटसबर्ग में एक विशाल भवन की चित्र-सज्जा भी की। इस समय की उनकी रंग योजनाओं में हरे, उन्नावी तथा फीके गुलाबी रंग के साथ सुनहरी रंग का प्रयोग हुआ है जो बडा ही प्रभावोत्पावक एवं लोकप्रिय हुआ।
रोरिक ने प्रकृति का चित्रण मानवीय क्रिया-कलापों के परिप्रेक्ष्य में ही किया है। उनके वृक्ष, पर्वत तथा मेघ सभी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने रूसी थियेटरों के लिये भी बहुत कार्य किया।
स्टेज सेटिंग, भित्ति चित्रण अथवा केनवास चित्रण सभी में रोरिक की प्रवृति आलंकारिकता की रही है। इसके साथ ही उनके रंग अत्यन्त व्यंजक है। उनके प्रिय रंग लाल, नीले, उन्नावी तथा सुनहरे पीले रहे हैं।
रोरिक ने अपने देश के बैले निर्माताओं के साथ मिलकर संगीत, चित्र आदि दृश्यात्मक कलाओं एवं अभिनय का सफल समन्वय भी प्रस्तुत किया है जो उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है तथा विश्वभर के नाट्यकर्मी जिससे प्रेरणा लेकर अपने-अपने क्षेत्र में इसी प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। सन् 1912 में रोरिक ने इस प्रकार का सर्वाधिक कार्य किया।
प्रथम महायुद्ध के समय रोरिक धार्मिक विषयों की ओर मुड़ गये किन्तु युद्ध से उत्पन्न सामाजिक पीड़ा ने भी उन्हें प्रभावित किया। इस समय तक रोरिक ख्याति के चरम शिखर पर पहुँच चुके थे।
1915 में उनका सम्मान किया गया और उनके चित्र अनेक संग्रहालयों में प्रदर्शित किये गये। उनके कला सम्बन्धी लेखों का 1914 में ही प्रकाशन हो चुका था। 1916 में वे बीमार हुए और चिकित्सा के लिये फिनलैण्ड चले गये।
इसी बीच 1917 में रूस की प्रसिद्ध अक्टूबर क्रान्ति हुई और वे अपने देश से कट गये। बाद में उन्हें कुछ देशों में रूसी कलाकृतियों की देखभाल का काम सपा गया।
वे अमेरिका भी गये। न्यूयार्क में उनके प्रशंसकों ने 1923 में रोरिक संग्रहालय की स्थापना की।
1920 में रोरिक ने मध्य एशिया तथा भारत के लिये दो पुरातात्विक अभियानों का कार्यक्रम बनाया। इनमें वे पामीर, मंगोलिया, तिब्बत तथा हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक इतिहास की खोज में निकले और 1928 में स्थायी रूप से कुल्लू के नगर में बस गये।
जीवन के अन्तिम 19-20 वर्ष उन्होंने यहीं व्यतीत किये। इस अवधि में हिमालय की विभिन्न छवियों ही उनके चित्रों में उभरती रहीं ।
अरुणोदय, सूर्यास्त, कुहरा. तेज धूप । और चाँदनी रात्रि में उन्होंने हिमालय की विभिन्न स्थितियों तथा स्थानों के अनेक चित्र बनाये। किन्तु ये चित्र केवल दृश्यांकन मात्र नहीं हैं बल्कि हिमालय की छाया में रहने वाले एक आध्यात्मिक कलाकार की उदात्त अनुभूति के ही विविध रूप हैं।
रोरिक इनके माध्यम से ब्रह्माण्ड के तत्व तक पहुंचना चाहते थे। इन चित्रों में नीला रंग अनन्तता की अनुभूति का प्रतीक बनकर चित्र तल पर प्रभादी रहता है। अन्य रंगों में श्वेत, गुलाबी, बैंगनी तथा हरितमणि के विविध बलों का प्रयोग है।
रोरिक के साथ पर्वतीय यात्राओं पर जाने वालों का कथन है कि हमें भले ही ये रंग अवास्तविक और विचित्र लगते हैं पर पर्वतीय ऊँचाइयों पर उन्हें वास्तव में देखा जा सकता है। इन्हें “ब्रह्माण्डीय” रंग कहा गया है।
कलाकार ने प्रकृति की शक्तियाँ को जीवन्त रूप में देखा है दूर आकाश के तारे तथा हिमाच्छादित रहस्यमय शिखर मनुष्य की पूर्णता प्राप्त करने की अनवरत कामना के प्रतीक हैं प्रकाश ज्ञान की शक्ति का सूचक है: सन्त तथा दार्शनिक आकृतियाँ मनुष्य की आध्यात्मिक जिज्ञासा की प्रतीक बनकर आयी हैं।
रोरिक की कला भारत के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गयी, चूँकि इसमें आध्यात्मिक प्रतीकता के साथ हिमालय का अंकन था।
भारत में उनकी बहुत प्रशंसा हुई और अनेक कलाकार, वैज्ञानिक तथा राजनीतिज्ञ उनका सम्मान करने लगे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक महापुरूष उनसे मिलने पहुँचते थे।
उनके चित्र संसार के अनेक संग्रहालयों में हैं तथा उनकी पुस्तकें इंग्लैण्ड, अमरीका एवं भारत में प्रकाशित हुई हैं।
15 दिसम्बर 1947 को 73 वर्ष की आयु में रोरिक की मृत्यु हुई और उन्हें कुल्लू में ही दफना दिया गया। निकोलस रोरिक एक सच्चे साधनारत कलाकार थे ।
वे आधुनिक चित्रकारों के समान व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा में नहीं उतरे । उन्होंने कला को सर्वव्यापी ब्रह्माण्डीय शक्ति के साक्षात्कार का साधन माना था। इसीलिये उनकी कला मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के अधिक समीप है।
श्री निकोलस रोरिक के पुत्र श्री स्वेतोस्लाव रोरिक का जन्म भी यद्यपि रूस हुआ था किन्तु ये भी स्थायी रूप से भारत में बस गये।
श्री स्वेतोस्लाव रोरिक भी में अपने पिता के समान कलाकार होनेके साथ-साथ लेखक, कवि तथा वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने भी हिमालय की भव्यता के अनेक चित्र अंकित किये हैं।
साथ ही दक्षिण भारत तथा कुल्लू घाटी के जन जीवन को भी अपने चित्रों में रूपायित किया है। बाइबिल, श्रम पीड़ित मानवता तथा भारतीय इतिहास को भी चित्रित किया है।
अधिकाश भारतवासी उन्हें प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी के पति के रूप में जानते हैं। स्वेतोस्लाव के चिन्तन पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का गहरा प्रभाव है।
बंगलौर में 30 जनवरी 1993 को उनका देहावसान हो गया जहाँ वे पिछले 40 से अधिक वर्षो से रह रहे थे।
प्रो० वाल्टर लैंगहैमर
1937 में बम्बई आने से पूर्व प्रोफेसर लैंगहॅमर विएना (आस्ट्रेलिया) के स्टेट कालेज आफ आर्ट में कला-अध्यापन करते थे बम्बई के कला जगत् में वे व्यक्ति चित्रकार और दृश्य चित्रकार के रूप में विख्यात हुए ।
स्थानीय कलाकारों से उनका अच्छा परिचय था और उनके स्टुडियों में कलाकारों की भीड लगी रहती थी। वे विनम्र एवं दयालु स्वभाव के थे।
कला की दृष्टि से वे उत्तर- प्रभावववादी शैली के अनुयायी थे अतः जहाँ भारतीय कलाकार उनकी रंग योजनाओं और शैली से प्रेरणा लेते थे वहीं उनके कला-सम्बन्धी ज्ञान से कला-गोष्ठियाँ लाभान्वित होती रहती थीं।
कृष्ण हवलाजी आरा तथा सैयद हैदर रजा पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा रजा से उनके गुरू-शिष्य के सम्बन्ध थे।
प्रो० लैंगहेमर टाइम्स आफ इण्डिया के प्रकाशनों के भी आर्ट डाइरेक्टर थे। उनके अनेक चित्र टाइम्स आफ इण्डिया के उस समय के वार्षिक अंकों में प्रकाशित होते रहे हैं।
भारत के स्वतंत्र होने के उपरान्त बम्बई की कलात्मक गतिविधियों को आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत् से जोड़ने का काम जो कलाकार कर रहे थे उन्हें प्रो० लैंगहैमर से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला; विशेष रूप से अभिव्यंजनावादी कला के प्रचार में।